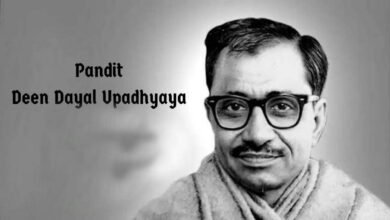क्या हमारा संविधान भारत को एक सूत्र में बांध रहा या बांट रहा?
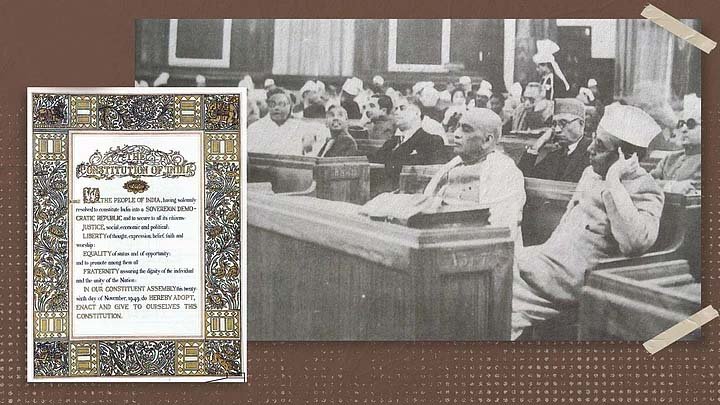
चूंकि भारत इस तरह के व्यापक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, जिसका मुख्य कारण यह है कि अमरीकन प्रणाली अपरिचित है और स्वदेशी नहीं है, इसलिए हमें अन्य सुधारों पर विचार करना चाहिए। जैसे कि, राष्ट्रपति का सीधे चुनाव करना और उनको अधिक विवेकाधीन अधिकार देना, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा का पुनर्गठन, या सांप्रदायिक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक अखिल समुदाय परिषद की स्थापना करना, इत्यादि…
हम भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यह समय उपयुक्त होगा कि हम ईमानदारी से मूल्यांकन करें कि यह एकता और सामाजिक सद्भाव को विकसित करने में विफल क्यों रहा है।
भारतीयों में एकता के अभाव के उदाहरण बहुत हैं… हिंदू-मुस्लिम हिंसा, जाति-आधारित राजनीति, उत्तर-दक्षिण विभाजन, भाषाई विवाद, कश्मीर और पंजाब में अलगाववादी आंदोलन, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में सशस्त्र विद्रोह, मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा, इत्यादि। चूंकि इनमें से कई संघर्ष आजादी के बाद से जारी रहे हैं और कई नए हैं, इसलिए एक राजनीतिक दल या नेताओं के एक समूह को दोष देना मुश्किल है।
इस तरह की व्यापक कलह भारत के शासन के तरीके में मूलभूत समस्या की ओर इशारा करती है। जब हमारे संस्थापकों ने 1950 में संविधान को अपनाया, उन्हें उम्मीद थी कि यह देश को एक साथ रखने वाले गोंद के रूप में काम करेगा। उन्होंने दस्तावेज में उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई विशेषताओं को शामिल किया …संसदीय निगरानी के साथ बहुमत-शासन, एकीकृत केंद्र के साथ राज्यों का संघ, धर्मनिरपेक्ष संरक्षण के साथ धर्म की स्वतंत्रता, और राष्ट्रीय भाषा थोपे बिना क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता।
संविधान की ये सभी तथाकथित एकीकृत विशेषताएं एकजुटता लाने में विफल रही हैं। बहुमत के शासन पर कोई संसदीय नियंत्रण नहीं है, केंद्र राज्यों पर हावी है, धर्मनिरपेक्ष संरक्षण अर्थहीन हो गए हैं, और भाषाई लड़ाई जारी है। आइए इनमें से प्रत्येक कमी की जांच करें।
अंतर्निहित बहुसंख्यकवाद बहुलवाद को नष्ट करता है
यह विचार कि संसद द्वारा बहुमत की सरकारों को नियंत्रित किया जाएगा, दो मुख्य कारणों से विफल रहा .. भारत की खंडित राजनीति, और इसकी संसदीय प्रणाली की सब शक्तियां विजेता (winner-take-all) को देने वाली प्रकृति।
भारत का राजनीतिक विखंडन काफी हद तक देश के स्थायी हिंदू बहुमत से उपजा है। चूंकि धर्म एकजुट करने की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, इसलिए हिंदू वोट स्वाभाविक रूप से समय के साथ एकजुट हो गया। विपक्ष के पास कुछ ही विकल्प बचे थे, उन्होंने तीन रणनीतियों का सहारा लिया : 1. हिंदू वोटों को जातीय आधार पर विभाजित करना, 2. क्षेत्रीय दल बनाना, या 3. अल्पसंख्यक समूहों को एकजुट करना। इसके परिणामस्वरूप एक खंडित राजनीतिक परिदृश्य पैदा हुआ, जिसमें कई पार्टियां देश को धर्म, क्षेत्र, या जातीय के आधार पर विभाजित करने में जुट गयीं।
इस मुद्दे को और जटिल बनाने वाली भारत की संसदीय प्रणाली है, जो बहुमत के नेता के हाथों में विधायी और कार्यकारी दोनों शक्तियों को सौंप देती है। प्रधानमंत्री, या राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों के हाथों में सत्ता का यह केंद्रीकरण, असहमति या अल्पमत की आवाजों को सुनने के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है।
छद्म संघवाद क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनदेखी करता है
संविधान भारत को ‘राज्यों का संघ’ के रूप में वर्णित करता है, जो सहकारी संघवाद और क्षेत्रीय विविधता के सम्मान का सुझाव देता है। व्यवहार में, हालांकि, प्रणाली केवल रूप में संघीय है और आत्मा में काफी हद तक एकात्मक है। राष्ट्रीय विखंडन के डर से, निर्माताओं ने एक ऐसी संरचना बनाई जिसमें केंद्र हावी है और राजकोषीय, विधायी और प्रशासनिक शक्तियों से राज्यों पर नियंत्रण रखता है।
समय के साथ, संवैधानिक संशोधनों और राजनीतिक परंपराओं ने इस असंतुलन को और भी आगे बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति, जिसकी मूल रूप से केंद्रीय कार्यकारिणी पर एक संभावित जांच के रूप में कल्पना की गई थी, प्रधानमंत्री के अधीनस्थ हो गए हैं। केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल अक्सर तटस्थ संवैधानिक प्राधिकारियों के बजाय पक्षपातपूर्ण एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।
इस केंद्रीय प्रभुत्व ने सहयोग के बजाय जबरदस्ती पर आधारित संघवाद का निर्माण किया है। नतीजतन, भारत को कई राज्यों में अलगाववादी आंदोलनों और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय विभाजन भी बढ़ रहा है। संवैधानिक विद्वान ग्रैनविल ऑस्टिन ने लिखा कि ‘‘अति-केंद्रीकरण ने केंद्र-राज्य संबंधों के लिए संविधान के कई प्रावधानों को असंतुलित कर दिया और एकता के कारण को पीछे धकेल दिया।’’ राज्य के मामलों में केंद्रीय हस्तक्षेप स्थानीय सरकारों को आंतरिक विवादों को हल करने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने की जिम्मेदारी से बचने की अनुमति देता है। मैंने पहले तर्क दिया है कि यह तथाकथित ‘मजबूत केंद्र’ कई राज्य-स्तरीय संघर्षों की जड़ है और हिंसक क्षेत्रीय आंदोलनों को हल करने में विफल रहा है। प्रारंभिक गणराज्य में उभरे अलगाववादी संघर्ष .. तमिल, सिख, कश्मीरी और नागा .. आज भी जारी हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह केवल तेज होता गया, अंतत: बिहार, झारखंड और अन्य क्षेत्रों में फैल गया। 2010 में, सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता ने कहा कि ‘‘1947 में स्वतंत्रता के बाद से भारत द्वारा लड़े गए पांच युद्धों की तुलना में आंतरिक असुरक्षा के कारण अधिक लोगों की जान गई है।’’
सतही धर्मनिरपेक्षता धार्मिक विभाजन को भडक़ाती है
धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का एक और स्तंभ है जो सैद्धांतिक रूप में महान प्रतीत होता है लेकिन निष्पादन में त्रुटिपूर्ण है। संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। परंतु भारत में धर्मनिरपेक्षता ‘धर्म और सरकार के बीच सख्त अलगाव’ पर आधारित नहीं, बल्कि ‘सभी धर्मों के लिए समान सम्मान’ पर आधारित है। व्यवहार में, इसने सरकार को धार्मिक मामलों में मनमानी से हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है। इस असमान दृष्टिकोण ने ‘तुष्टीकरण’ और ‘बहुसंख्यकवाद’ दोनों आरोपों को जन्म दिया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता में कौन है।
इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता ने धार्मिक पहचान को बेअसर करने के बजाय, अक्सर इसका राजनीतिकरण किया है। चुनावी राजनीति नियमित रूप से सांप्रदायिक विभाजन का फायदा उठाती है। एक तटस्थ सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने से दूर, संवैधानिक ढांचे ने धर्म को एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बने रहने में सक्षम बनाया है, जिससे सामाजिक दरार गहरी हो गई है।
आज, भारत अपनी विश्व प्रसिद्ध सदियों पुरानी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को खोने का जोखिम उठा रहा है। कई भारतीय विचारक अभी भी मानते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता जीवित रह सकती है यदि सरकारें सभी धर्मों से ‘सैद्धांतिक दूरी’ बनाए रखें, या उन्हें समान रूप से बढ़ावा दें। लेकिन वे राजनेताओं को नहीं पहचानते और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं।
भाषाई विभाजन
भाषा हमेशा भारतीयों में अलग पहचान का एक परिभाषित मार्कर रही है, और संविधान द्वारा इसे संभालना लगातार तनाव का स्रोत रहा है।
निर्माताओं ने हिंदी और अंग्रेजी को ‘आधिकारिक भाषाओं’ के रूप में नामित करते हुए किसी भी एक राष्ट्रीय भाषा को घोषित करने से परहेज किया। इस समझौते ने तत्काल अशांति को तो रोका, परंतु इसने भाषाई विभाजन को भी मजबूत किया।
एक स्पष्ट राष्ट्रभाषा के अभाव ने प्रतीकात्मक स्तर पर भारत की एकता की भावना को नुकसान पहुंचाया है। उन देशों के विपरीत जहां भाषा एक साझा पहचान के रूप में कार्य करती है, भारत का बहुभाषावाद खंडित करता है।
भारत के विकल्प
कुल मिलाकरए ये विशेषताएं .. मजबूत केंद्र, छद्म संघवाद, सतही धर्मनिरपेक्षता और भाषाई अस्पष्टता .. एक पैटर्न को प्रकट करती हैं। संविधान को विविधता का संरक्षण करने की बजाय इसे नियंत्रित करने के लिए अधिक डिजाइन किया गया था।
भारत अपने संविधान में इन कमजोरियों की अनदेखी कर अपना ही नुकसान कर रहा है। उन्हें ठीक करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते हमारे नेता संविधान का लगातार गुणगान करने के बजाय लोगों को इन कमियों के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करें।
धर्मनिरपेक्ष और भाषाई खामियों को संबोधित करना सबसे सरल है क्योंकि वे संरचनात्मक नहीं हैं। संसद सरकारों को किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि में शामिल होने से रोकने के लिए एक कानून पारित कर सकती है, और एक कानून राष्ट्रीय भाषा स्थापित कर सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों में पहले से ही ऐसे कानून हैं। संरचनात्मक समस्याओं .. अंतर्निहित बहुसंख्यकवाद और छद्म संघवाद .. को अधिक मौलिक परिवर्तनों की आवश्यकता है। एक विकल्प, जिसका मैंने लंबे समय से समर्थन किया है, अमेरिकी शैली की राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाना है। यह मॉडल विधायी और कार्यकारी शक्तियों को अलग करता है और शक्तियों के तीन अलग-अलग केंद्र बनाता है .. राष्ट्रपति, सीनेट और हाउस .. जो अल्पसंख्यकों को अधिक प्रभाव देते हैं। यह स्वतंत्र सरकार की दो परतें भी प्रदान करता है .. संघीय और राज्य .. जो स्थानीय समुदायों को अधिक नियंत्रण प्रदान करता है।
चूंकि भारत इस तरह के व्यापक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, जिसका मुख्य कारण यह है कि अमरीकन प्रणाली अपरिचित है और स्वदेशी नहीं है, इसलिए हमें अन्य सुधारों पर विचार करना चाहिए। जैसे कि, राष्ट्रपति का सीधे चुनाव करना और उनको अधिक विवेकाधीन अधिकार देना, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा का पुनर्गठन, या सांप्रदायिक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक अखिल समुदाय परिषद की स्थापना
करना, इत्यादि।
सबसे बढक़र, भारत को हमारे संविधान की खामियों के बारे में एक ठोस और ईमानदार बहस की आवश्यकता है। हमें एक महान लोगों के योग्य संविधान की मांग करनी चाहिए।-भानु धमीजा